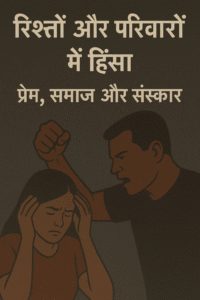हम जिनसे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं – वही जब हमारे लिए डर और दुःख का कारण बनें, तो इंसान अंदर से टूट जाता है।
रिश्तों और परिवारों में हिंसा एक ऐसा विषय है, जो अक्सर हमारे समाज में अनदेखा, अनकहा और अस्वीकार्य माना जाता है – फिर भी यह वास्तविकता है, और लाखों परिवारों की रोज़मर्रा की कहानी।
इस निबंध में हम समझेंगे:
- रिश्तों और पारिवारिक हिंसा के स्वरूप क्या हैं?
- क्यों होता है ऐसा?
- संस्कार, समाज और प्रेम की भूमिका क्या है?
- और इसका समाधान कैसे निकले?
1. रिश्तों में हिंसा: परिभाषा और प्रकार
पारिवारिक या घरेलू हिंसा (Domestic Violence) का अर्थ केवल शारीरिक मारपीट नहीं है। यह एक मानसिक, भावनात्मक, आर्थिक, यौन और सामाजिक नियंत्रण की प्रक्रिया भी हो सकती है।
मुख्य प्रकार:
- शारीरिक हिंसा: मारपीट, धक्का-मुक्की, बाल खींचना, जलाना, चोट पहुँचाना
- मानसिक/भावनात्मक हिंसा: ताने, अपमान, नीचा दिखाना, चुप कराने की धमकी
- यौन हिंसा: जबरन यौन संबंध, मर्यादाओं का उल्लंघन
- आर्थिक हिंसा: पैसे पर नियंत्रण, खर्च के लिए तरसाना, कमाई न करने देना
- सामाजिक हिंसा: बाहर जाने से रोकना, लोगों से मिलने से मना करना
हिंसा केवल पति-पत्नी के बीच नहीं, बल्कि माता-पिता, बच्चों, सास-ससुर, बहु, भाई-बहन जैसे किसी भी पारिवारिक रिश्ते में हो सकती है।
2. सांख्यिकी और समाजिक यथार्थ
भारत जैसे देश में घरेलू हिंसा एक मौन महामारी की तरह फैल चुकी है:
- राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के अनुसार, हर 3 में से 1 महिला अपने जीवनकाल में किसी न किसी रूप में घरेलू हिंसा का शिकार होती है।
- पुरुषों के विरुद्ध घरेलू हिंसा के मामले भी बढ़ रहे हैं, लेकिन वह रिपोर्ट नहीं होते क्योंकि “मर्द रोते नहीं” की मानसिकता हमें रोकती है।
यह हिंसा सिर्फ किसी जाति, धर्म, शिक्षा या वर्ग तक सीमित नहीं – अमीर, पढ़े-लिखे, शहरी परिवारों में भी यह उतनी ही गहराई से जमी है।
3. यह हिंसा क्यों होती है? कारणों की तह में जाएं
3.1 पितृसत्ता (Patriarchy) और नियंत्रण की मानसिकता
हमारे समाज में पुरुष को घर का मालिक, निर्णयकर्ता और महिला को उसकी “प्रॉपर्टी” मानने की परंपरा रही है।
यह मानसिकता जब चुनौती दी जाती है (जैसे महिलाएं काम करने लगें, अपनी राय रखें) – तो वही पुरुष हिंसा का सहारा लेने लगता है।
3.2 संस्कारों का दोषपूर्ण पक्ष
हम ‘संस्कार’ के नाम पर कई बार यह सिखाते हैं कि:
- लड़की को सब सहना चाहिए
- परिवार की बदनामी नहीं होनी चाहिए
- पति चाहे जैसा हो, उसे देवता मानो
यह गलत संस्कार पीड़ित को चुप कराते हैं, अपराधी को बढ़ावा देते हैं।
3.3 बचपन का प्रभाव और ट्रॉमा
जिस बच्चे ने बचपन में हिंसा देखी है, वह बड़ा होकर उसी व्यवहार को दोहराता है – चाहे वह शिकार बना हो या गवाह।
जब जीवन में असफलता या तनाव बढ़ता है, तो व्यक्ति उसे बाहर निकालने के लिए कमजोर रिश्तों का सहारा लेता है – जो सबसे पास होते हैं, उन पर ही गुस्सा निकलता है।
3.5 नशा और असंयम
शराब, ड्रग्स या अन्य नशे की हालत में विवेक कमजोर हो जाता है। तब छोटी बातों पर भी हिंसा हो जाती है।
4. संस्कार: निर्माण या विनाश?
संस्कार का अर्थ है – जो सिखाया गया हो, जो हमारे आचरण में हो।
क्या हम सही संस्कार दे रहे हैं?
हम कहते हैं:
- “लड़का चाहे जितना गुस्सैल हो, लड़की को समर्पित रहना चाहिए।”
- “बीवी की बात मानी तो मर्द नहीं कहलाओगे।”
- “बेटी घर की इज़्ज़त है, बदनामी नहीं होनी चाहिए – भले मारपीट होती हो।”
इन बातों में कहीं प्रेम, सम्मान, बराबरी की जगह नहीं है।
संस्कार अगर किसी को डर और अपमान में जीने के लिए मजबूर करें – तो वे संस्कार नहीं, संवेदनहीनता हैं।
5. प्रेम: जहाँ प्रेम है, वहाँ हिंसा नहीं हो सकती
5.1 सच्चे प्रेम की परिभाषा
प्रेम वह है:
- जहाँ आज़ादी हो, डर नहीं
- जहाँ सहयोग हो, आदेश नहीं
- जहाँ संवाद हो, चुप्पी नहीं
- जहाँ उन्नति हो, बंधन नहीं
यदि कोई कहे: “मैं तुझसे प्यार करता हूँ, इसलिए तुझे मारता हूँ।” – तो वह प्रेम नहीं, आत्मिक अत्याचार है।
5.2 रिश्तों में प्रेम की जगह कब खत्म होती है?
जब अहंकार, स्वार्थ, नियंत्रण, ईर्ष्या और संदेह प्रेम की जगह ले लेते हैं – तब रिश्ते हिंसा में बदल जाते हैं।
6. बच्चों पर इसका प्रभाव: एक पीढ़ी बर्बाद हो जाती है
अगर बच्चा रोज़ देखे:
- पिता मां को मारता है
- मां चुपचाप सहती है
- अपमान सामान्य है
तो वह क्या सीखेगा?
या तो वो एक दिन पीड़ित बनेगा, या अत्याचारी।
“हम अपने बच्चों को उपदेश नहीं देते – हम उन्हें अपना व्यवहार देकर संस्कार देते हैं।”
7. समाधान: समाज, कानून, और व्यक्तिगत स्तर पर बदलाव
7.1 सामाजिक परिवर्तन जरूरी है
- स्कूलों में भावनात्मक शिक्षा, रिश्तों की समझ
- बच्चों को जेंडर बराबरी का पाठ पढ़ाना
- पंचायत/समुदाय स्तर पर घरेलू हिंसा पर खुली चर्चा
7.2 क़ानूनी प्रावधान
भारत में महिलाओं की सुरक्षा के लिए कई कानून हैं:
- धारा 498A (IPC): दहेज और क्रूरता के मामलों के लिए
- घरेलू हिंसा अधिनियम (2005): जिसमें मानसिक, आर्थिक, यौन सभी प्रकार की हिंसा शामिल है
- महिला हेल्पलाइन (181), पुलिस सहायता, NGO, लीगल ऐड
लेकिन कानून तभी कारगर होंगे, जब पीड़िता बोलेगी – और उसे समर्थन मिलेगा।
7.3 पुरुषों के लिए भी प्लेटफ़ॉर्म
कई पुरुष भी घरेलू हिंसा के शिकार होते हैं – लेकिन शर्म, समाज और कानून के डर से बोल नहीं पाते।
समाज को दोनों लिंगों के लिए न्यायपूर्ण और सहायक वातावरण बनाना होगा।
8. क्या करें यदि आप पीड़ित हैं?
- स्वीकार करें: हिंसा कोई सामान्य बात नहीं है
- बोलें: परिवार, दोस्त, NGO, कानून – कहीं तो आवाज़ उठाएँ
- सबूत रखें: मैसेज, वीडियो, मेडिकल रिपोर्ट, गवाह
- स्वावलंबी बनें: नौकरी, शिक्षा, आत्मनिर्भरता
- काउंसलिंग लें: मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें
9. क्या करें अगर आप हिंसक हैं?
- स्वीकार करें: यह आपके अंदर की समस्या है
- माफी माँगें और बदलाव का संकल्प लें
- काउंसलिंग और थेरेपी लें
- संयम, योग, मेडिटेशन से अभ्यास करें
- रिश्तों को प्रेम, संवाद और विश्वास से पुनर्निर्माण करें
निष्कर्ष: प्रेम, संवाद और समानता ही रिश्तों की नींव होनी चाहिए
रिश्तों का आधार यदि हिंसा है, तो वह रिश्ता नहीं, बंधन है।
संस्कार यदि चुप्पी सिखाएं, तो वे समाज के अपराधी हैं।
प्रेम वह शक्ति है जो किसी को गुलाम नहीं बनाती – बल्कि आज़ाद करती है।
“जहाँ डर है, वहाँ प्रेम नहीं रह सकता।
जहाँ प्रेम है, वहाँ कोई स्थान हिंसा का नहीं है।”
हर परिवार एक छोटा सा समाज है। अगर हम घरों को प्रेममय, सम्मानपूर्ण और सुरक्षित बना दें – तो आने वाली पीढ़ियाँ अहिंसा, सह-अस्तित्व और प्रेम की मिसाल बनेंगी।